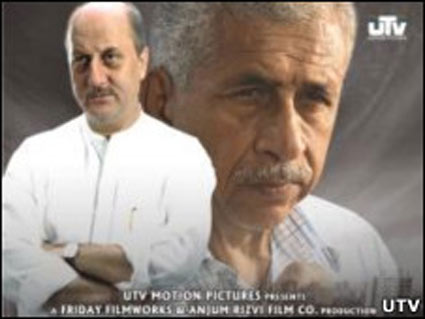सरकारें जनता पर सख़्त हुईं और अलग-अलग समुदाय के लोगों की आपसी नरमी कम हो गई। हमला अमरीका में हुआ, लेकिन उसने पूरी दुनिया में चरमपंथ, धर्म और विश्वास की परिभाषाएं हिला कर रख दीं। पिछले दशक में बदले इस सामाजिक परिवेश पर अमरीका का फ़िल्म उद्योग कुछ ख़ामोश ही रहा। लेकिन बॉलीवुड ने अपना दायरा बढ़ाते हुए इसे पहचाना और बड़ी बेबाक़ी से कई फ़िल्मों के ज़रिए बड़े पर्दे पर एक नया दृष्टिकोण रखा।
फिल्म आलोचक नम्रता जोशी के मुताबिक़, "जहां पश्चिमी देशों में बनी फ़िल्मों ने इस हादसे को ज़िंदगी बदलने वाले एक निजी अनुभव की तरह देखा, वहीं बॉलीवुड ने इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदली राजनीति और एक ख़ास समुदाय पर उसके असर को दिखाया। चाहे वो ‘माइ नेम इज़ ख़ान’ में राष्ट्रपति को मुस्लिम समुदाय की ओर धारणा बदलने को कहना या “न्यूयॉर्क” और “आमिर” फ़िल्म में उदारवादी मुसलमानों का चित्रण, जिसे भारत के बाहर, ख़ास तौर पर अरब देशों में बहुत सराहा गया."
'मेरा नाम ख़ान है और मैं आतंकवादी नहीं हूं'
साल 2010 में रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘माइ नेम इज़ खान’ में हीरो की मां उसे मज़हब के आधार पर लोगों में फ़र्क करने से रोकती हैं और कहती हैं– इस दुनिया में सिर्फ़ दो किस्म के इंसान हैं, अच्छे इंसान जो अच्छा काम करते हैं और बुरे इंसान जो बुरा काम करते हैं, बस यही एक फ़र्क है इंसानों में।
इस फ़िल्म में 11 सितंबर के हमले के बाद के माहौल में यहीं अंतर हीरो अमरीका के राष्ट्रपति को समझाने की कोशिश करता है, ये कह कर कि– माइ नेम इज़ ख़ान एंड आई एम नॉट ए टेररिस्ट यानी मेरा नाम ख़ान है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। फ़िल्म में एक प्रेम कहानी के ज़रिए अमरीका में रह रहे एशियाई मूल के लोगों की ज़िंदगी की बदली परिस्थितियों को दिखाया गया है।
11 सितंबर के हमलों के बाद हिंदू और ईसाई धर्म के लोगों का मुसलमानों की ओर रवैया, अमरीकी सुरक्षा एजेंसियों का धर्म के मुताबिक़ संदेह करना, यहां तक कि एक पति और पत्नी के रिश्ते में बनी ख़ाई।
फिल्म की पटकथा लिखने वाली शबीना बथीजा कहती हैं कि ये फ़िल्म अहम है। उन्होंने कहा, "इस दौर में जो इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है और जिसके परिणाम आम लोगों को भुगतने पड़ रहे हैं, वो दिखाना और कुछ परेशान करने वाले सवाल पूछना भी बहुत ज़रूरी था."
अलग मुसलमान चेहरा
11 सितंबर के हमलों को बड़े पर्दे पर दिखाने वाली पहली बड़ी फिल्म थी। वर्ष 2009 में रिलीज़ हुई– ‘न्यू यॉर्क’। न्यूयॉर्क में रह रहे तीन दोस्तों की कहानी ‘न्यूयॉर्क’ 11 सितंबर के हमलों के बाद के हालात दिखाती है। निर्देशक क़बीर ख़ान के मुताबिक़ उन्होंने इस फ़िल्म के लिए बहुत शोध किया, जिस वजह से वो अपनी कहानी को सच्चाई के बेहद क़रीब ला सके।
फ़िल्म में साफ़ तौर पर अमरीकी ख़ुफिया एजेंसी को निर्दोष लोगों को ग़ैर-क़ानूनी ढंग से हिरासत में रखने और यातनाएं देते हुए दर्शाया गया है और इसके कारण उन्हीं निर्दोष लोगों को बदले की भावना में चरमपंथ की ओर क़दम बढ़ाते हुए भी।
फ़िल्म के लेखक संदीप श्रीवास्तव कहते हैं, "फ़िल्में आपके आसपास के समाज का ही प्रतिबिम्ब होती हैं, हमने वही दिखाया जो उस दौरान लोगों को परेशान किया। आपके महज़ किसी धर्म से जुड़े होने की वजह से आपको आतंकवदी करार दिया जाए तो ये कितना बड़ा लांछन है."
11 सितंबर के हमलों के बाद के दौर में न्यूयॉर्क में फ़िल्माइ गई फ़िल्म ‘क़ुर्बान’ भी वर्ष 2009 में ही रिलीज़ हुई। ‘न्यूयॉर्क’ से अलग, इस फ़िल्म में आम मुसलमानों के चरमपंथ का रास्ता अपनाने की वजह किसी निजी अनुभव को नहीं बताया गया, बल्कि इसे एक बड़ी अंतरराष्ट्रीय समस्या के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई।
फ़िल्म में एक अमरीकी विश्वविद्यालय की कक्षा में एक मुसलमान छात्र और कुछ अमरीकी छात्रों के बीच बहस के ज़रिए ये उभारने की कोशिश की गई है कि अमरीका को आतंकवादी हमलों का निशाना इसलिए बनाया गया है, क्योंकि उसने राजनीतिक और सैन्य तरीक़ों से और देशों में दख़लंदाज़ी की।
भारत में छोटे बजट की फ़िल्में
‘माइ नेम इज़ खान’ की ही तरह, ‘क़ुर्बान’ और ‘न्यूयॉर्क’ की कहानी भी, भारत में नहीं फिल्माई गई थी। लेकिन 11 सितंबर के बाद बदला माहौल भारत में भी कई बदलाव लाया। ऐसा नहीं कि बॉलीवुड के फिल्मकारों ने अपने घर में पड़ रही दरारों से किनारा कर लिया हो।
वर्ष 2008 में रिलीज़ हुई एक बेहद अहम फिल्म ‘अ वेडनसडे’। जिसमें एक आम आदमी का ख़ौफ़, ग़ुस्सा, उलझन और व्यवस्था से हताशा बख़ूबी दिखाई गई। हालांकि फिल्म ‘रंग दे बसंती’ की तरह ‘अ वेडनसडे’ में सुझाया गया रास्ता भी क़ानून के दायरे के बाहर था।
वर्ष 2008 में ही आई फ़िल्म ‘आमिर’। एक थ्रिलर होने के बावजूद ये फ़िल्म इस्लाम धर्म और चरमपंथ पर एक बेहद संजीदा और सहज बहस को सामने लाई।
इसके बाद उसी वर्ष रिलीज़ हुई फ़िल्म ‘मुंबई मेरी जान’। मुंबई में लोकल ट्रेनों पर हुए सिलसिलेवार बम धमाकों पर आधारित इस फ़िल्म में पांच आम ज़िंदगियों की आपबीती दिखाई गई- उनका दुख, उनका डर, उनकी झुंझलाहट और असमंजस।
फ़िल्म आलोचक नम्रता जोशी कहती हैं कि ये फ़िल्में चाहे छोटे या बड़े बजट की हों, बॉक्स ऑफिस पर हिट या फ़्लॉप रही हों और चाहे इनमें सुझाए गए रास्ते पूरे तरीक़े से सही और सहज ना हो, पर बॉलीवुड ने उदारवादी मुसलमान को आवाज़ देकर दुनिया के सामने एक अलग दृष्टिकोण ज़रूर दिया है।
International News inextlive from World News Desk